अगर मैं गोदान लिखता? लेकिन निश्चय है मैं नहीं लिख सकता था, लिखने की सोच भी नहीं सकता था। पहला कारण कि मैं प्रेमचंद नहीं हूँ, और अंतिम कारण भी यही कि प्रेमचंद मैं नहीं हूँ। वह साहस नहीं, वह विस्तार नहीं। गोदान आसपास ५०० पृष्ठों का उपन्यास है। उसके लिए धारणा में ज्यादा क्षमता चाहिए, और कल्पना में ज्यादा सूझबूझ। वह न होने से मेरा कोई उपन्यास ढाई सौ पन्नों से ज्यादा नहीं गया। मैं लिखता ही तो गोदान करीब दो सौ पन्नों का हो जाता। गोदान का एक संक्षिप्त संस्करण भी निकला है और मानने की इच्छा होती है कि उसमें मूल का सार सुरक्षित रह गया है। यानी दो सौ-ढाई सौ में भी गोदान आ सकता था। और क्या विस्मय, मोटापा कम होने से उसका प्रभाव कम के बजाय और बढ़ जाता, अब यदि फैला है तो तब तीखा हो जाता।
पुस्तक जब शुरु में निकली थी तभी मैंने पढ़ी थी। याद पड़ता है, प्रेमचंद ने एक अगाऊ प्रति भेज दी थी। यह कोई अठारह वर्ष पहले की बात है। तब से पुस्तक की कथा मन पर कुछ धुंधली हो आई थी। उस, समय मैंने लिखा था कि गाँव की कथा पर उसमें शहर कुछ थोपा हुआ-सा है, वह अनिवार्य नहीं है, पुस्तक की कथा के साथ एक नहीं है। हो सकता था कि होरी को कथा के केंद्र में रखने के लिए, और ऐसे ही सब प्रकाश उसी पर पड़े, दूसरे ब्योरे ध्यान को खींचकर अपनी ओर न ले जाएँ, शहर को पुस्तक से मैं अनुपस्थित हो जाने देता। ऐसा संभव था कि शहरी जीवन के प्रति विरोध और अनास्था प्रकट करने का सुभीता न रहता, न ग्रामीण जीवन के प्रति रुचि और सहानुभूति को उबारने का उस प्रकार सुगम अवसर। लेकिन मैं उसका लोभ न करता। कैसे कहूँ कि प्रेमचंद को लोभ का संवरण करना चाहिए था? क्योंकि यह प्रतिपादन तो कदाचित प्रेमचंद की प्रेरणा में मुख्य तत्व बनकर रहा है। लेकिन मेरी फिर भी धारणा है कि गाँव और शहर की तुलना और जय-पराजय से अलग करके होरी का चित्रण उतना विविधतापूर्ण और रंग-बिरंग चाहे न बनता, फिर भी उसमें अधिक व्यक्तित्व और एकत्व हो सकता था। अठारह वर्षों बाद वह पुस्तक अब फिर जहाँ-तहाँ से देख गया। तब की धारणा नष्ट नहीं हुई, बल्कि पुष्ट ही हुई। हठात शहर ने आकर पुस्तक के गाँव को चमकाया नहीं है, बल्कि कहीं कुछ बखेरने और ढकने का प्रयास किया, ऐसा प्रतीत हुआ।
किताब में एक-पर-एक पात्र आते गए हैं। उनकी संख्या पर विस्मय होता है। होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, हीरा, सोभा, सोना और रूपा तो एक परिवार के ही हैं। भोली, दुलारी, झिंगुरी साहू, दातादीन, मंगरू साहू, पटेश्वरी, मातादीन, वगैरह भी आसपास के लोग हैं। शहर के राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा, मिर्ज़ा, मालती आदि आज की नई सभ्यता के लोग हैं। मानना होगा कि खासा मेला है, अगरचे सबका उसमें अपना-अपना रंग और अपनी व्यक्तिमत्ता है, उनका चित्र सामने आ जाता है। लेकिन शायद मैं होता तो सबको न छूता, दो-चार को लेकर ही काम चला लेता। कुछ तो इसलिए कि मेरा बस उतना ही है; कुछ इसलिए भी कि संख्या की अधिकता अवगाहन में सहायक नहीं होती, गहनता विस्तार में छिप जाता है और दृश्य रूप अदृश्य गुण से प्रधान हो जाता है। उससे समाज और समय का चित्र तो मिलता है, पर आत्म की उतनी गहरी अनुभूति कदाचित प्राप्त नहीं होती। मुझे ठीक मालूम नहीं कि साहित्य का क्या लक्ष्य है, वह हमें वस्तु-बोध देने के लिए है कि आत्म-प्रकाश देने के लिए? साहित्य का जो भी इष्ट और उद्दिष्ट हो, स्वीकार करना चाहिए कि मेरी अपनी रूचि विविध जानकारियों के प्रति उतनी नहीं है, न परिचय के विस्तार के प्रति। परिचय अधिक से न हो किंतु अभिन्नता कुछ से भी हो तो मुझे यह बड़ा लाभ जान पड़ता है। गहरा मित्र एक हो तो उसकी कीमत सौ जान-पहचान वालों से मेरे लिए ज्यादा हो जाती है। निश्चय प्रेमचंद हमें बहुत देते हैं, इतनी तरह-तरह की जानकारियाँ देते हैं कि हम समा नहीं सकते। लेकिन एक दूसरे तरह की उपलब्धि भी है। बौद्धिक से उसे आत्मिक कहा जा सकता है। वह व्यथा की सघनता के रूप में मिलती है। मैं लिखता तो मेरी इच्छा रहती कि मैं उसका ध्यान विशेष रखूँ।
प्रेमचंद भाषा के जादूगर हैं, मुहावरे उन्हें सिद्ध हैं। भाषा का यह खेल और यह प्रभाव उन्हें याद से नहीं उतरता। इससे जगह-जगह प्रयोग ऐसे आ जाते हैं जो अपने खातिर और सिर्फ चमक के लिए आये लगते हैं। जैसे एक जगह है- “पुन्नी हाय-हाय करती जाती और कोसती जाती थी, तेरी मिटटी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आ जाए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएन्ज़ा हो जाए, तू कोढ़ी हो जाए, हाथ-पाँव कट-कट गिरें…”
दूसरी जगह: “होरी मिनका तक नहीं, झुँझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खुला, आँख जली, दाँत पिसे” इत्यादि।
ऐसे प्रयोग बहुत हैं। यह उनके वर्णन की शैली है। जैसे शब्द अपनी खूबी के जोर से बाहर आते और बैठते जाते हैं। मैं होता तो संकेत से काम लेता। “पुन्नी हाय-हाय करती जाती और कोसती जाती थी”, इसके बाद बिना कुछ कहे रह जाता। इसमें निश्चय ही हानि हो जाती, चित्र की यथार्थता उतनी न खिलती, लेकिन मुझे स्वीकार होता।
‘पुन्नी ने हाय-हाय की और कोसा’, यह कहने के बाद उस विलाप को फिर और नाना दुर्वचनों से सचित्र और सांगोपांग करने से मैं किनारा ले जाता। मनोदर्शन और विश्लेषण में मैं कुछ निश्चित कहने और प्रतिपादन करने से बचता। ज्ञान आखिर हमारा अनुमान है। क्या उसके आगे प्रश्नचिन्ह नहीं है? इससे कैफियत भर देता, निदान नहीं।
रायसाहब के पीछे होरी चलता है और राय साहब बैठकर अपनी गाथा शुरु करते हैं। कहते-कहते वह अपनी स्थिति की बखिया खोलते चले जाते हैं, “हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है। हमारे लोग मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हों। अरे और तो और, हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई तो इसी रियासत के बल पर मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और ऐयाशी कर रहे हैं… आज मर जाऊँ तो घी के चिराग जलाएँ। मेरे दुःख को दुःख समझनेवाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुःख की हँसी उड़ाता हूँ। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। ब्याह कर लूँ तो विलासान्धता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो यह मेरी कमजोरी है, शराब पीने लगूँ तो यह प्रजा का रक्त होगा। अगर ऐयाशी नहीं करता तो अरसिक हूँ। ऐयाशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या है! इन लोगों ने मुझे भोग-विलास में फँसाने के लिए कम चलें नहीं चलीं और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊँ, और ये मुझे लूट लें। और मेरा धर्म यह है कि सब-कुछ देखकर भी कुछ न देखूँ, सब कुछ जानकार भी अंधा बना रहूँ।”
इस तरह राय साहब कहते ही जाते हैं। रायसाहब काउन्सिल के मेंबर हैं, बड़े आदमी हैं। होरी रायत नाचीज़ हैं। लेकिन दो पन्नों तह वह नहीं रुकते, और मुँह पान से भरकर फिर आगे कहते हैं, “हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे हैं।” और इस तरह समाजशास्त्र और तत्त्वशास्त्र की भी चर्चा करते चले जाते हैं। कहते हैं, “दुनिया समझती है, हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर-चाकर, क़र्ज़, वेश्याएँ, क्या नहीं हैं? लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुःख पर सब हँसे और रोनेवाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैर के नीचे दबी हो, जो भोग-विलास के नशे में अपने को भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने आधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कह सकता।” …रायसाहब कहते ही जाते हैं और दो पन्ने और भर जाते हैं!
इस लंबे उदगार का प्रयोजन यह है कि आगे उन्हीं को गुस्सा होते और उससे बिलकुल उल्टा आचरण करते दिखाया जाए। मुझे लगता है कि शब्दों को उतना सोच न पाता, उनके प्रयोगों से मैं ज़ल्दी हार जाता। मैं मानता हूँ कि शब्दों को कहीं चुक जान चाहिए। बुद्धि की भाषा ही शाब्दिक है, व्यथा मौन द्वारा बोलती है। प्रेमचंद में वहाँ भी शब्द मुखर हैं, जहाँ मैं उनसे हार मान बैठता और शब्द हीनता में सहारा ले रहता।
प्रेमचंद में प्रेम का व्यापार भी शब्दों से उतना मुक्त नहीं है। गोबर किशोर है और सामने झुनिया को पाता है। झुनिया छोटी-सी थी तभी ग्राहकों के घर दूध ले जाया करती थी। ससुराल में भी उसे गाहकों के घर दूध पहुँचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह-तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। दो-चार रुपए हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मँगनी की चीज़ हो; इसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती है। यह झुनिया खूब बात करती है। कहती है, ‘तुम मेरे हो चुके, कैसे जानूँ?’ गोबर ने कहा, ‘तुम जान भी चाहो तो दे दूँ।’ ‘जान देने का अर्थ भी समझते हो?’ ‘तुम समझा भी दो न’, ‘जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र-भर निबाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ-बाप, भाई-बंद, घर-द्वार सब कुछ छोडना पड़े। मुँह में जान देनेवाले बहुतों को देख चुकी, भौंरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे!’
आगे भी वह कहती जाती है, ‘एक से एक ठाकुर, महाराज, बाबा, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फँसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, ‘झुनिया तरसा मत।’ कोई मुझे रसीली-नशीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र-भर, बल्कि उस जन्म भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौंरे हैं, रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कराती हूँ। वे मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ।’
नहीं, निश्चय ही कैशोर प्रेम को मैं किसी भी तरह इतना प्रगल्भ, इतना हिसाबी, इतना मुखर न बना सकता। प्रेम की विवशता और स्वच्छन्दता में और कितना भी आगे मैं बढ़ता लेकिन किसी भी प्रकार इतना सशब्द न हो सकता। जीवन के पहले प्रेम में ये शब्द यदि किसी और से सुन मिलते कि ‘वह गधी बनाते हैं मैं उल्लू बनाती हूँ’, तो मेरी कलम फिर किसी तरह वहाँ प्रेम को टिका न पाती।
मन-मान्यताओं से भी लिखने का संबंध रहता है। शायद वह संबंध सीधा तो नहीं होता पर चरित्र-चित्रण में आ ही जाता है। होरी के गाँव में जितने नेता हैं, सब धूर्त हैं और धार्मिक हैं। धर्म का और धूर्तता का वैसा गठजोड़ मेरे मन में उतना निश्चित नहीं है। धूर्तता सब में है और धर्म की आवश्यकता भी सब में है। इसलिए एक में दोनों चीज़ें मिलें, इसमें कुछ भी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन उसमें कार्य-कारण का संबंध देख लेना मेरे बस का न हो पाता। प्रेमचंदजी जैसे इसी आविष्कार तक जा पहुँचे हैं। पंडित दातादीन, लाला पटेश्वरी, ठाकुर झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम सब ही एक-न-एक रूप में भक्ति-उपासना में समय देते हैं, लेकिन उसी कारण जैसे दुखिया के दुःख के प्रति वे और भी हृदयहीन हो जाते हैं।
मैं उनके स्वाभाव को ज्यों-का त्यों रखकर भी शायद प्रेमचंद के निदान से सहमत न होता। धर्म सीधा धूर्तता उपजाता हो तो जैसे समस्या बहुत सीधी हो जाती है और उतने सीधे चलकर मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे संतोष हो सकता है।
संक्षेप में, गोदान में जो होरी निपट भाग्य के सामने अकेला जूझता हुआ फिर भी निरुपाय-सा दिखता है, मैं उसको तो न छूता और ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रखता। फिर भी भाग्य को किन्हीं तात्कालिक परिस्थितियों अथवा व्यक्तियों से परिभाषा देने का प्रयत्न न करता कि जैसे होरी शिकार हो, शिकारी दूसरे हों। मेरी कोशिश होती कि दिखाता कि सब जैसे शिकार ही हैं और वृथा ही एक-दूसरे को शिकार बनाने का प्रयत्न करते हैं! असल में शक्तियाँ निर्वैयक्तिक हैं और उनमें सत् के साथ रहने और असत् के साथ लड़ने के लिए सहानुभूतियों का बँटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा मैं कर सकता तो मानता कि मेरा ‘गोदान’ सफल है।
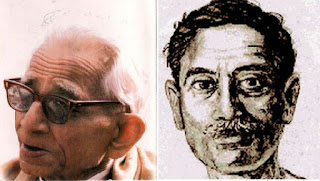
अप्रतिम लेख।उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद