2004 में प्रदर्शित ‘द डे आफ्टर टूमारो’ में पर्यावरण संकट के भयावह रूप को दिखाया गया था। यद्यपि यह एक काल्पनिक कथा थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में यह कल्पना जिस तेजी से यथार्थ में रूपांतरित होने की ओर बढ़ी है, वह कहीं से भी उस फिल्म की कहानी से कम भयावह नहीं है। वैश्विक तापन के कारण ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से लेकर विश्व के भू जल संभरों (Aquifiers ) में जल का निरंतर घटता स्तर इस विश्वव्यापी समस्या की महज बानगी है। सपाटबयानी से काम लें तो कह सकते हैं, समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर और प्रलयंकारी हो सकती है, जितनी ‘द डे आफ्टर टूमारो’ में कल्पना की गई है। 1950-1960 के दशक में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को विज्ञान-कथाओं (Science Fictions) में भी खूब जगह मिली। इन कथाओं में शहरों के डूबने से लेकर महासागरों के सूखने तक की आशंकाएँ व्यक्त की गईं।
समस्या की भयावहता के सामने आने के साथ-साथ निश्चित तौर पर इसके प्रति चिंताओं में भी वृद्धि हुई है। सरकारी-गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त बुद्धिजीवियों ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जनमत तैयार करने की कोशिश की है। इसी चिंता का परिणाम है कि पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दे विज्ञान-कथाओं से निकल कर थ्रिलर की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। सारा मोस (Sarah Moss ) की ‘कोल्ड अर्थ’ और मैथ्यू ग्लास की ‘अल्टीमेटम’ उस नए जेनर के उपन्यासों के उदाहरण हैं, जिसे ‘इकोलाजिकल थ्रिलर’ का नाम दिया गया है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिन्दी में इस जेनर में ज्यादा काम नहीं हुआ। इस दृष्टि से श्री रमाकांत मिश्र और डॉक्टर सबा खान का हालिया उपन्यास ‘महासमर: परित्राणाय साधूनाम् एक उल्लेखनीय कृति मानी जानी चाहिए। यह न सिर्फ इस जेनर में एक अभाव की पूर्ति करता है, बल्कि एक प्रतिमान भी स्थापित करता है, जिसे छूना इस जेनर के भावी लेखकों के लिए एक कठिन चुनौती होगी।
उपन्यास के पहले पृष्ठ पर ही लेखक द्वय स्वर्गीय रवींद्र जैन की पंक्ति ‘जल जो न होता तो ये जग जाता जल’ उद्धृत कर यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी चिंताओं के केंद्र में सम्पूर्ण विश्व को तेजी से अपनी चपेट में लेता ‘जल-संकट’ है। 2015 में अपने उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नासा (NASA) ने यह घोषणा की कि संसार के 37 बड़े जल-संभरों (Aquifiers) में से 21 का जल खत्म होने के कगार पर है। इस घोषणा ने ‘जल-युद्ध’ की संकल्पना को एक यथार्थ आधार दे दिया है, जिसके अनुसार, अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए लड़ा। जाएगा।
महासमर इसी जल-संकट को केंद्र में रखकर रचा गया एक इकोलाजिकल थ्रिलर है। उपन्यास का कलेवर विस्तृत है। कथा एक साथ कई अलग-अलग रेखाओं में आगे बढ़ती है। इससे आरंभ में एक विशृंखलता-सी दिखती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूत्र जुड़ते नजर आने लगते हैं और आरंभ में समानांतर-सी दिखती कथा रेखाएँ एक बहुकोणीय ज्यामितीय संरचना का निर्माण करने लगती हैं।
कहानी पर्यावरण संकट और उससे जुड़ते अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तारों के बीच अपना ताना-बाना बुनती हुई आगे बढ़ती है। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त डेंगू, चिकनगुनिया, पोलिओ और जीका वायरस के नमूने और इनके प्रसार में किसी मानवीय हस्तक्षेप की आशंका इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े कर देती है। जाँच की शुरुआत में ही साजिशकर्ताओं की पहुँच का अंदाजा लग जाता है, जब न सिर्फ जाँच से जुड़ा एजेंट अचानक लापता हो जाता है, बल्कि अहम सबूतों के साथ कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क भी गायब कर दिए जाते हैं।
साजिश कई स्तरों पर रची जा रही थी। बिहार के सुपौल में एक नवनिर्मित बाँध न सिर्फ पहली बारिश में ही बह जाता है, बल्कि अपने साथ-साथ एक रिसर्च इंस्टिट्यूट को भी बहा ले जाता है। इस घटना की जाँच के क्रम में एक पत्रकार को बाँध के टूटने ही नहीं, बनने में भी साजिशों के तार दिखते हैं। पत्रकार इस साजिश के खुलासे के लिए जैसे ही गहराई में जाने की कोशिश करता है, उसकी अपनी जान के ही लाले पड़ जाते हैं।
राजनीतिक छल-छद्म, भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी से लेकर अप्रत्यक्ष जैविक युद्ध की साजिशों के बीच से आड़ी-तिरछी बढ़ती इस कथा में पाकिस्तान की आई एस आई (ISI) की सक्रिय भागीदारी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्रदान करती है।
रहस्य और रोमांच के बीच उपन्यास काफी तेज गति से आगे बढ़ता है। 400 से अधिक पृष्ठों की यह यात्रा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह पाठकों को अपने साथ यूँ लिए चली जाती है कि रोमांच एक क्षण को भी कम होता नहीं लगता। उपन्यास के आखिरी पृष्ठ पर पहुँच कर आप एक लंबी जोर की साँस लेते हैं, लेकिन यह राहत की अनुभूति बस क्षणिक होती है। आपको अचानक ध्यान आता है कि उपन्यास का एक भाग और है और तमाम रहस्यों के धागे अभी पूरी तरह उलझे हुए हैं। आप दुबारा पढ़ चुके पन्नों को पलटने लगते हैं कि शायद किसी रहस्य का कोई सिरा कहीं हाथ लग जाए, लेकिन इस कोशिश में धागे और उलझने लगते हैं और आप थक हार कर उपन्यास को वापस रख देते हैं।
रहस्य और रोमांच से इतर बात करें तो बहते पानी के समान सहज-सरल भाषा इसकी एक और उपलब्धि है, जो पात्रों और क्षेत्रों के साथ-साथ रंग बदलती चलती है। पात्रों के नामकरण में भी लेखकद्वय ने विशिष्टता दर्शाई है और उन्हें कथा से जुड़े प्रतीकों के रूप में चित्रित किया है। उदाहरण के लिए प्रदूषण नामक पात्र को देख सकते हैं, जो जल-संकट से जुड़ी साजिश के एक महत्वपूर्ण पुर्जे के रूप में सामने आता है। उपन्यास चूँकि दो भागों में लिखी गई महाकाय गाथा का पहला भाग है, इसलिए प्रतीकों के सम्पूर्ण अर्थ और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए दूसरे भाग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसका आगमन अगले महीने अपेक्षित है।
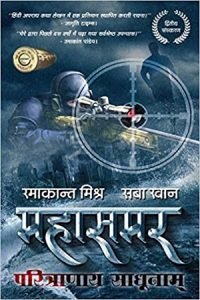
बेहतरीन विश्लेषण सिन्हा साहब। बधाई